

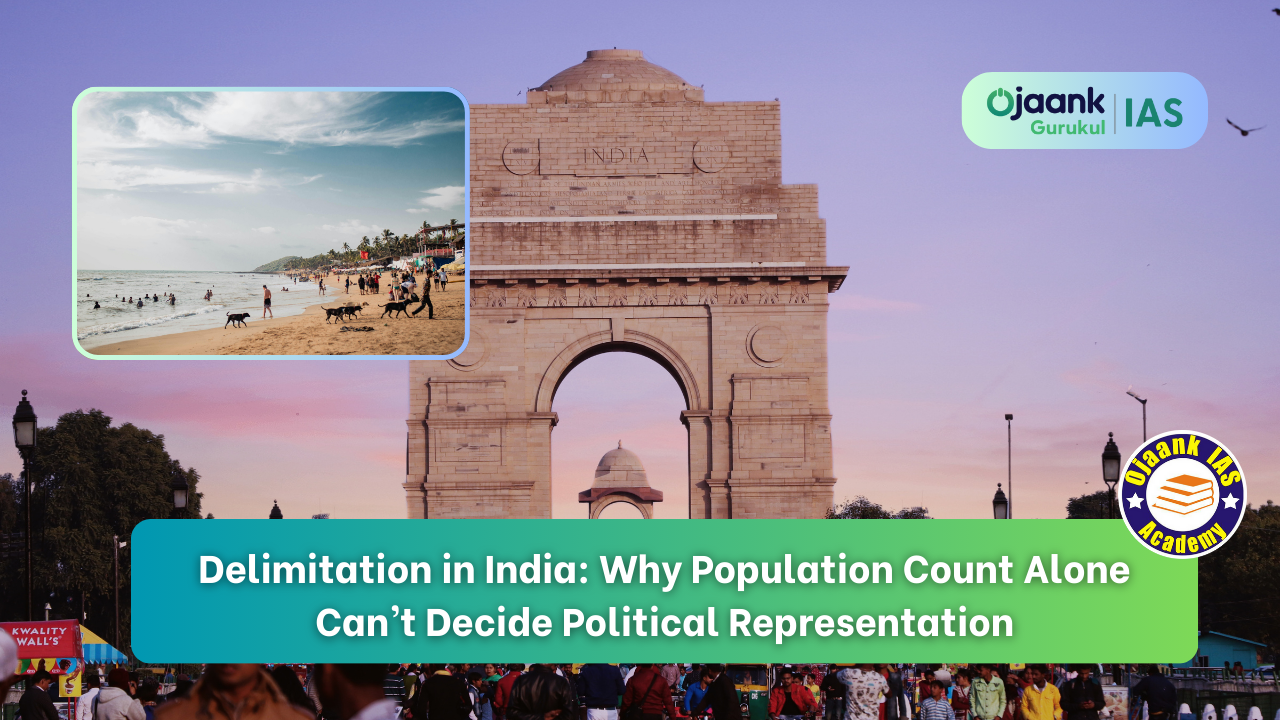
जैसे-जैसे 2026 में लोकसभा सीटों के आवंटन पर संवैधानिक फ्रीज़ की समाप्ति निकट आ रही है, प्रतिनिधित्व, संघीय समानता और जनसांख्यिकीय न्याय की रेखाएं और गहरी हो रही हैं। आगामी परिसीमन अभ्यास ने संसद और राज्य विधानसभाओं में गंभीर बहस को जन्म दिया है, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, जो जनसांख्यिकीय प्रगति के बावजूद राजनीतिक रूप से कम प्रतिनिधित्व की आशंका जता रहे हैं।
क्या केवल जनसंख्या ही राजनीतिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण और संसाधनों के आवंटन का उचित आधार है? अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी कसौटी पर सवाल उठाएं और एक अधिक समावेशी जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण अपनाएं।
1951 से 1971 के बीच, भारत में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती जनसंख्या के जवाब में बढ़ाई गई। यह अनुपात 1951 में प्रति सीट 7.3 लाख लोगों से बढ़कर 1971 में 10.1 लाख हुआ, जब सीटों की कुल संख्या 543 तक पहुंच गई।
हालाँकि, 2026 तक परिसीमन पर लगी रोक के चलते जनसंख्या वृद्धि ने संसदीय विस्तार को पीछे छोड़ दिया है। 2026 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार, भारत में 753 लोकसभा सीटें होनी चाहिए, जिनमें औसतन 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हो।
लेकिन यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है—यह इस बात पर है कि कौन और कितनी न्यायसंगत तरीके से प्रतिनिधित्व पा रहा है।
🌐 भारत में 1976 से लोकसभा सीटों की संख्या क्यों स्थिर है?
जानिए: संसदीय सीट आवंटन का इतिहास और भविष्य।
उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आज भी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं, जबकि दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, और कर्नाटक ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है—स्वास्थ्य और शिक्षा के मजबूत मॉडल के माध्यम से।
यदि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय होगा, तो ये सफल राज्य दंडित होंगे जबकि पीछे छूटे राज्य लाभ उठाएंगे—यह एक विडंबना है।
यह विरोधाभास 15वें वित्त आयोग के दौरान सामने आया, जब वित्तीय वितरण के लिए 1971 के बजाय 2011 की जनगणना का उपयोग किया गया। आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को एक अतिरिक्त मानक के रूप में जोड़ा, जिससे अधिक जनसंख्या और कम प्रदर्शन वाले राज्यों और कम जनसंख्या और बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों के बीच संतुलन बना।
🌐 उत्तर और दक्षिणी राज्यों पर परिसीमन का असमान प्रभाव
एक्सप्लोर करें: कैसे जनसंख्या वृद्धि भारत की संघीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है।
यह मानना आसान है कि जनसंख्या जितनी अधिक होगी, प्रतिनिधित्व उतना अधिक होना चाहिए। लेकिन यह सोच कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करती है:
जनसंख्या घनत्व
जनसांख्यिकीय संक्रमण
शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन
स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम
बुनियादी ढांचे की क्षमता
वर्तमान में, पूर्वोत्तर भारत इसका उदाहरण है, जहां कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को भी पर्याप्त सीटें दी गई हैं। क्या यही सिद्धांत पूरे देश में लागू नहीं होना चाहिए?
जनसंख्या घनत्व को गाइडिंग फैक्टर मानना एक उचित "मध्य मार्ग" हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च घनत्व और कम जनसंख्या वाला जिला शायद एक बड़े लेकिन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र से अधिक प्रतिनिधित्व का हकदार हो सकता है।
🌐 कैसे जनसांख्यिकीय प्रदर्शन सीट आवंटन को प्रभावित करना चाहिए?
जानें: शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरी के लिए राज्यों को पहचान देने की आवश्यकता।
सरकार की एक बड़ी भूल यह है कि वह प्रति व्यक्ति आँकड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहती है—प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय, प्रति व्यक्ति शिक्षा बजट।
यह आंकड़े यह नहीं बताते कि लोग कौन हैं और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। यह “प्रति व्यक्ति भ्रामकता” विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में खतरनाक है, जहां तुलनाएं असमानताओं को नजरअंदाज करते हुए की जाती हैं।
केवल जनसंख्या को हर मानक के हर डिनॉमिनेटर में रखने से यह मान लिया जाता है कि सभी की ज़रूरतें समान हैं—जो कि विज्ञान और न्याय दोनों का उल्लंघन है।
🌐 भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना
अधिक जानें: क्यों चुनावी पुनर्वितरण को सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।
जनसंख्या की जनसांख्यिकीय पढ़ाई केवल गिनती नहीं है। यह समझने की प्रक्रिया है कि:
आयु संरचना क्या है
लैंगिक संतुलन कैसा है
जातीय और सामाजिक समूहों का वितरण
आर्थिक निर्भरता की दरें
सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच
इन गुणों को ध्यान में रखकर हम एक सार्थक मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं—जो विविधता, असमानता और जीवन की सच्चाई को सम्मान देता है।
यह विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां जाति और लिंग पहले से ही निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे में एक समान दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व को विकृत कर सकता है।
🌐 प्रतिनिधित्व में जाति, लिंग और सामाजिक-आर्थिक कारकों की भूमिका
और पढ़ें: कैसे सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को चुनावी वितरण में शामिल किया जाना चाहिए।
भारत निम्नलिखित तरीकों से परिसीमन के लिए जनसंख्या के पार जाकर सोच सकता है:
प्रति सीट प्रतिनिधित्व की सीमा तय करें: यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या 20 लाख से कम हो।
जनसंख्या घनत्व को आधार बनाएं: पूर्वोत्तर की तरह, भूगोल और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी प्रतिनिधित्व में महत्व दें।
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को मान्यता दें: बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
संरचना को संख्या पर वरीयता दें: उम्र, जाति, लिंग और आर्थिक संरचना को प्रतिनिधित्व के मानकों में शामिल करें।
संघीय समानता को बनाए रखें: प्रतिनिधित्व का निर्णय संविधान की संघीय भावना के अनुरूप हो, जिससे किसी क्षेत्र का वर्चस्व न हो।
2026 का परिसीमन कोई साधारण प्रशासकीय अभ्यास नहीं है—यह भारत की न्यायसंगत शासन की प्रतिबद्धता की परीक्षा है। यदि प्रतिनिधित्व केवल जनसंख्या संख्या से तय होगा, तो क्षेत्रीय असमानताएं और अधिक बढ़ेंगी और संघीय व्यवस्था कमजोर होगी।
जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उसके ढांचे भी आगे बढ़ने चाहिए। चलिए, गिनती से इंसानियत की ओर बढ़ें। चलिए, संख्यात्मक कठोरता के बजाय जनसांख्यिकीय बुद्धिमत्ता अपनाएं। और चलिए यह सुनिश्चित करें कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि न्याय में भी बड़ा हो।
जनसंख्या मार्गदर्शक हो सकती है, लेकिन निर्णायक नहीं होनी चाहिए। भारत के संघवाद का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।
कॉपीराइट 2022 ओजांक फाउंडेशन